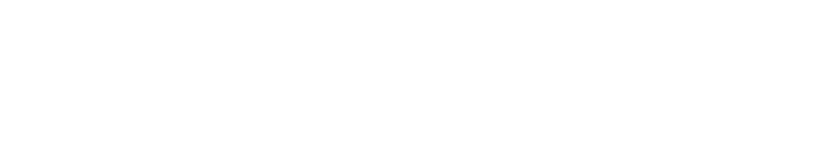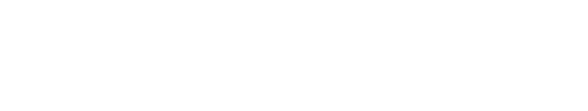आमपौर पर (अधिकतर) हमारी ज़बानों से एक वाक्य सुनने को मिलता है रवासिमे अज़ा (रीतियाँ) मरासिमे अज़ा (प्रथाऐं) जिसका अर्थ हर वह कार्य होता है जिसका सम्बन्ध अज़ादारी से हो।
शाब्दिक दृष्टि से रस्म (रीति) के विभिन्न अर्थ होते हैं इनमें शक्ल, सूरत, निशान, अलामत (चिन्ह) के साथ साथ तरीक़ा (विधि) क़ानून, नीति, आदत आदि भी हैं।
जिसमें अच्छे, बुरे, ग़लत, सही की कोई क़ैद नही है और न ही धर्म, जाति, वंश की शर्त बल्कि हर वह बात और काम जो आदत (स्वभाव) में शामिल हो जाये रस्म (रीति) कहलाने लगता है।
इसमें इसकी कोई शर्त नही है कि वह लाभदायक है या हानिकारक आवश्यक या अनावश्यक, इसलिये ऐसी समस्त प्रचलित विधियाँ जिनको रस्म (रीति) कह कर याद किया जाता है अनावश्यक समझ लिये जाते हैं। बल्कि अकसर उन पर यह ऐतेराज़ (आपत्ति) भी हो जाते हैं ऐसी अवस्था में प्रश्न यह उठता है कि
इमाम हुसैन (अ) की अज़ा (शोक) में शोक प्रक्रट करने के लिये जो तरीक़े प्रयोग में आते हैं, यह भी परम्परा है और अज़ा ए इमाम हुसैन (अ) के बारे में हमारे सम्त कार्य, कथन, बिल्कुल महत्व नही रखते हैं इसलिये कि अगर हम उसको महत्व दें तो अपने अरकाने अज़ा (स्तम्भ) मरासिमे अज़ा (परम्परा) न कहा करते।
वास्तव में अभी हमने यही निर्णय नही लिया है कि अज़ादारी एक रस्म (परम्परा) है या इबादत। स्पष्ट है कि अगर अज़ादारी को हम रस्म समझते हैं होंगे तो अज़ा के तमाम तरीक़े रवासिम (रीतियाँ) मरासिमे अज़ा (प्रथाऐ) ही कहे जायेंगें।
लेकिन अगर अज़ा रस्म नही बल्कि इबादत है तो उससे सम्बन्धित सभी कार्य, मरासिम (परम्परा) नही बल्कि उस इबादत के अंश और स्तम्भ होंगे बात केवल एहसास की है अगर हमारा तहतुश शुऊर (अवचेतना) किसी वास्तविकता से प्रभावित है तो लाशऊरी तौर पर (......) उससे सम्बन्धित कार्यों में उसके प्रभाव मिलेंगे।
अत: अगर इबादत के बारे में भी परम्परा जैसे शब्दों का उपयोग किया जाये तो इबादत अपनी वास्तविकता से हट कर रस्म (परम्परा) बन जायेगी और हम इबादत के महत्व और सम्मान से बिल्कुल वंचित हो जायेंगे। उदाहरण स्वरूप ईद मनाना हमारी ऐसी इबादत है जो इस्लाम की महत्वपूर्ण इबादत है।
यहाँ कि वह दिन जो ईद का दिन कहलाता है इतना महान है कि हम ईद की नमाज़ के क़ुनूत में बार बार हाथ उठा कर ईद के दिन के माध्यम से अल्लाह से सवाल करते हैं और कहते हैं
कि माबूद आज के दिन के सद़के (उपलक्ष) में कि जिसे तूने मुसलमानों के लिये ईद बनाया और हुज़ूरे अकरम (स) के लिये उस दिन को महान,
अभिमान पूर्वक भंडार और निरंतर सहमती का सूत्र बनाया है (मेरा सवाल यह है कि) मुहम्मद व आले मुहम्मद (स) पर रहमतें व बरकतें नाज़िल फ़रमा और मुझे उस अच्छाई में
शरीक फ़रमा ले जिसमें तूने मुहम्मद व आले मुहम्मद (अ) को शरीक फ़रमाया है दुआ की अजम़त (महानता) का कौन अंदाज़ा (अनुमान) लगा सकता है कि क्या माँगा जा रहा है
और किससे माँगा जा रहा है और किस वली (अभिभावक) के सदक़े (माध्यम) से माँगा जा रहा है अब इस इतनी महान और अहम (महत्वपूर्ण)
इबादत के साथ बर्ताव मुलाहेज़ा (अवलोकन) फ़रमाऐं। यह इबादत वास्तव में रस्म (रीति) बन कर रह गई है क्योकि इस इबादत के साथ इबादत का तसव्वुर (कल्पना) अलग कर दिया गया है
तो उसके बाहरी और दाख़ली (आंन्तरिक) अरकान (अंग) इबादत का अंश होने के बजाए रस्म (परम्परा) हो गये
अब ख़ुद अपने दिल से सवाल कीजिये कि क्या यह नये कपड़े पहनना इबादत है या रस्म (परम्परा), यह गले मिलना इबादत है या रस्म (परम्परा), यह ख़ुशी मनाना इबादत है
या रस्म (परम्परा), यह बच्चों को ईदी देना इबादत है या रस्म, यह ख़ुशी का इज़हार (प्रकटी करण) इबादत है या रस्म, स्पष्ट है कि हमने जब इबादत के समस्त अरकान (स्तंम्भ) को रस्म बना कर अमल किया तो आने वाली नस्लों (वंश) ने ईद को रस्म के रुप में मनाना शुरु कर दिया।
अत: अब ख़ुशी मनाने के हर मुसलमान ने साधारण रुप से वाजिब मान लिया है कि वह ईद के दिन ख़ुशी प्रकट करे, अब जैसे वह मुसलमान मुसलमान नही जो ताश खेलने का कर्तव्य न निभाये,
घर में गाने बजाने का प्रोग्राम न रखे क्योकि आज ईद है टी वी के प्रोग्राम न देखे क्योकि आज ईद है। यह सब कुछ एक इबादत के अरकान (स्तंम्भ) को रस्म की नीयत (उद्देश्य) से अदा करने का क़हरी परिणाम है। आज ईद के दिन आप हर जगह के मुसलमान का जायज़ा (अवलोकन) लीजिए मुहर्रमात (अवैध) का पालन जैसे वाजिब (अनिवार्य) बन गया है और कुछ तो कुछ वाजिबे ऐनी (सब के लिये अनिवार्य) की सीमा तक मुलाज़िम (अत्युकति) में ग्रस्त है
बस इसी भयानक ख़तरे से सबक़ लेते हुए एक सवाल अज़ादाराने इमामे मज़लूम (अ) के सामने रखने की जसारत (दु:साहस) की जा रही है कि पहले फ़ैसला (निर्णय) करके बयाऐं कि अज़ाऐ इमामे मज़लूम वह इबादत होने की वजह से अंजाम देते हैं या उसको रस्मी मुज़ाहेरात (प्रदर्शन) समझ कर अंजाम देते हैं।
स्पष्ट है कि वह शिया जो जो नाम के शिया हैं उनके लिये मुमकिन (संभव) है कि वह अज़ाऐं इमाम (अ) को रस्मी मुज़ाहेरा कह दें, वर्ना वास्तविक अज़ादार ख़्वाब में भी इसकी जसारत (दु:साहस) नही कर सकता नही करेगा कि अज़ादारी की
कल्पना वह इबादत से हट कर कर सके फिर उसका यह धार्मिक कर्तव्य होगा कि वह इस इबादत का विस्तार पूर्वक अवलोकन करे कि इस इबादत के अरकान (स्तम्भ) क्या हैं ताकि अय्यामे अज़ा में होटलों और ज़रदोज़ी के कारख़ानों में रिकार्डिंग के बजाए नौहों की कैसिटों और नौहों की तिलावत के वक़्त सीने पर मातम की आवाज़ के बजाए किसी साज़ की मुशाबेह (समान) आवाज़ के बारे में इतमीनान (संतोष) किया जा सके कि यह एक इबादत है कोई परम्परा नही, हमें विश्वास है कि आप ख़ुद एक तवील (दीर्ध) सूची ऐसे मालूमात (नित्यकार्यों) की तैयार करेंगें जिसमें गंभीरता नाम की कोई चीज़ नही है
जिनके सम्बन्ध में कुछ कहना आपको शिईयत के मेयार (स्तर) से ख़ारिज (बाहर) कर दे। उदाहरण स्वरुप एक शिया बस्ती में जुलूस में शिरकत (भाग लेने वाले लोग ख़ुलूस व अक़ीदत (शुध्द हृदयता व श्रध्दा) के साथ रसूल (स) की तअस्सी (अनुसरण) में नंगे पैर, नंगे सर रहते हैं
और जुलूस जब किसी अज़ाख़ाने में प्रवेश करता है तो अज़ादार भी अज़ाखाने में ज़ियारत (दर्शन) के लिये प्रवेश करके ज़ियारत (दर्शन) करते हैं लेकिन यह बात भूल जाते हैं कि हम अभी ग़लाज़त (अपवित्रता) भरी सड़कों और गलियों की कीचड़ में पैर काले करके आ रहे हैं
और इमामबाड़े की सीमा कि जिसको पवित्र रखना हम पर अनिवार्य है हमारे अपवित्र पैरों से उसका अपमान होगा लेकिन इससे ज़्यादा ख़तरनाक (शिक्षा प्रद) बात यह है कि टोकने वाला ज़ईफ़ुल ईमान भत्सर्ना का पात्र बना गया और ताविलात (अर्थापन) के नये नये ज़ाविये (कोण) सामने खड़े कर दिये गये। इसी तरह क़दम क़दम पर हमने हुस्ने अक़ीदत (श्रध्दा) के मुताज़ाद (विपरीत) अम्बार अपना लिये हैं।
बहरहाल हमें यह बात हर समय ज़हन (मस्तिक) में रखना वाजिब (अनिवार्य) है कि अज़ादारी एक इबादत है नमाज़ रौज़े जैसी इबादत यह किसी तरह का सियासी (राजनीतिक) मुज़ाहेरा (प्रदर्शन) नही है, अज़ा को ठुकरा कर हमारी नमाज़ें लश्करे यज़ीद की नमाज़ों से तो मुशाबेह हो सकती हैं लश्करे हुसैनी की नमाजों के मुशाबेह नही हो सकतीं है।
इसलिये हमको अज़ा के लिये नमाज़ की तरह बल्कि उससे भी ज़्यादा ...... रास्ता अपनाना होगा
source : alhassanain